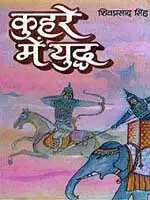|
सामाजिक >> कुहरे में युद्ध कुहरे में युद्धशिवप्रसाद सिंह
|
421 पाठक हैं |
|||||||
प्रस्तुत है रोचक उपन्यास...
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
इस उपन्यास में अधिकतर पात्र ऐतिहासिक है और इसमें इतिहास की समृद्ध
परम्परा प्रभावी ढंग से मुखर हुई है तथा वर्तमान की दारुण स्थितियों का भी
सजीव चित्रण है।
यह उपन्यास दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में प्रस्तावित नाम ‘हनोज दिल्ली दूर अस्त’ था, यही फोलियो पर छपा है। बाद में इसी का नाम ‘कुहरे में युद्ध’ करना पड़ा जो अधिक उपयुक्त है। यह उपन्यास अपने में स्वतंत्र खंड है। इसी उपन्यास का पूरक खण्ड ‘दिल्ली दूर है’ नाम से उपलब्ध है।
यह उपन्यास दो भागों में विभाजित है। पहले भाग में प्रस्तावित नाम ‘हनोज दिल्ली दूर अस्त’ था, यही फोलियो पर छपा है। बाद में इसी का नाम ‘कुहरे में युद्ध’ करना पड़ा जो अधिक उपयुक्त है। यह उपन्यास अपने में स्वतंत्र खंड है। इसी उपन्यास का पूरक खण्ड ‘दिल्ली दूर है’ नाम से उपलब्ध है।
आभार
इस खण्ड के लेखन में पर्याप्त साहित्य पढ़ना पड़ा। कई-कई वस्तुओं के बारे
में जानने की हरचन्द कोशिश की, पर अब भी अनेक त्रुटियां होंगी खासतौर से
भाषा में। मेरी द्वितीय मातृ भाषा उर्दू रही है, पर मुद्दत पहले जो पढ़ा
था, वह भूल चुका इसलिए वाक्य-विन्यास आदि की कतिपय भूलें हैं, किन्तु वे
भूलें वैसी ही हैं जैसी मध्यकालीन इतिहास को दृष्टि-बिन्दु में रखकर लिखने
वाले मेरे पूर्वज हिन्दी कथाकारों में हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर
आश्वस्त हूं कि अरबी-फारसी शब्दों का कोष्ठकों में अर्थ देखकर समझ लेंगे।
एक शब्द टेढ़ा सा बिना हिन्दी अर्थ के घुसा है पृष्ठ 207 पर वह है अंदलीब।
यह नाम है एक सुरीली चहकती चिड़िया का। कुछ इसे बुलबुल भी कहते हैं। मैंने
भाषा की कठिनाई तोड़ दी है। अतः उनके पाठक भी मेरे पाठकों के साथ इसके
रसास्वादन में आनन्द अनुभव करेंगे। बुन्देलखंड की धरती कई बार की
देखी-पहचानी है पर भूगोल और कतिपय नगरों के नामादि के बारे में बहुमूल्य
सूचनाएं उरई के डॉ. रामशंकर द्विवेदी से प्राप्त हुई हैं। मैं उनका कृतज्ञ
हूं। वे इधर निकट तर होते गए हैं इसलिए कृतज्ञता प्रकाश भी औपचारिकता ही
है। सम्बन्धों का तो मूल्य नहीं होता। शंकर टंकणालय के श्री अनिल कुमार
श्रीवास्तव ने मेरी अपठनीय पांडुलिपि को टंकित करके छपने योग्य बनाया है,
वे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। राजपाल एण्ड संज़ के विश्वनाथजी का कृतज्ञ
हूं। उन्होंने इस उपन्यास को प्रूफ की कम-से-कम गलतियों के साथ छापकर बहुत
अच्छे ढंग से मेरे पाठकों, के सामने प्रस्तुत किया है। निर्णय तो मेरे
नए-पुराने पाठकों के हाथ है, मेरा कार्य जैसा हुआ आपके सामने है। आप अपना
खुद संभालें। विदा पुनर्मिलनाय-
-शिवप्रसाद सिंह
रुकिए, आगे भग्नावशेष हैं
धेरा और इतिहास लगभग मिलते-जुलते अभिप्राय वाले विरोधी शब्द लगते हैं पर
इसमें शक नहीं कि हम जब भी भारतीय वातावरण में अतीत को देखना चाहते हैं,
वर्तमान को पहचानने के लिए या इसके आगे भविष्यत् की ओर बढ़ने के लिए हमारा
इतिहास एक मोटी पर्त जैसा लगता है जो सत्य के मुख को हिरण्यमय पात्र से
ढंकने की, ढंके रखने की छद्म-प्रक्रिया छोड़ने को तैयार नहीं लगता। मुझसे
बार-बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आप ‘अलग-अलग
वैतरणी’ के बाद काशी पर क्यों लिखने लगे या कि ‘नीला
चांद’ की सफलता ने क्या आपको लाचार बना रखा है कि आप आज के
समसामयिक परिवेश से टकराना नहीं चाहते ? मैं अब कैसे समझाऊँ कि यह प्रश्न
कथा-साहित्य को बाड़े-बन्दी में कैद रखने वाले अधकचरे समीक्षकों की लाचारी
से उपजा है जो हिन्दी-कथा-क्षेत्र में ग्रामीण, आंचलिक, मनोवैज्ञानिक,
ऐतिहासिक आदि शीर्षकों में उपन्यास-साहित्य को बाँट कर आसान समीक्षाएं
लिखने में लगे हुए हैं। ऐसे समीक्षकों में अधिकांश मुदर्रिस हैं, मेरे
जैसे ही। मैं कृति साहित्यकार की मुहर अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहता,
पर निवेदन जरूर करूंगा कि ये चौखटे तोड़िए। आप अगर आज भी उपन्यासों पर
कुंजियां लिखने में तल्लीन रहना चाहते हैं तो रहें, पर पाठक और लेखक के
बीच सेतु बनने या बनाने की अभीप्सा हो तो आप ना, न देखकर शिविर और
गोलबन्दी से प्रभावित हुए बिना उस लेखक की रचना की तह में जाने की कोशिश
कीजिए। साहित्य में रचनात्मकता तब मरती है जब अन्तस्तल से रस सोखकर वृक्ष
की शाख-शाख में, डाली-डाली में, पत्ते-पत्ते में जड़े संजीवनी भेजना बन्द
कर देती हैं।
यही स्थिति आज न केवल साहित्य बल्कि भारतीय समाज के हर क्षेत्र में परिलक्षित होती है। सच तो यह है कि हम अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके नये ढंग से अपने को किंचित् बदल कर या वातावरण के अनुकूल अपने को परिवर्तित करके समस्वरता स्थापित करने की प्रक्रिया ही भूल गये हैं। इसी कारण हमारा अतीत शुष्क, वर्तमान दरारों से भरा और भविष्य सूखे पेड़ की तरह निष्पत्र और नंगा लग रहा है। समीक्षा अगर एक बड़ी चीज को समझने में दस वर्ष का समय मांगती है तो मुझे पूर्णतः स्वीकार है, पर मैं उन मुदर्रिसों से लड़ना नहीं चाहता जो विश्वव्यापी कथा-साहित्य से शतप्रतिशत दूर होने को अपना भूषण मानते हैं। अगर आपको निरन्तर सिकुड़ती पृथ्वी की साम्प्रतिक स्थित की सहज प्रतीति नहीं है तो मैं अपने को अपराधी क्यों मानूं ? मेरे लिए प्रेमचन्द अब मंजिल नहीं हैं, उसी तरह मैं प्रसाद को अस्वीकार करना सत्य से आंखे चुराना कहता हूं। आचार्य द्विवेदी के चारों उपन्यास मेरे संबल हैं। क्योंकि प्रसाद और प्रेमचन्द की संधि की एक अद्भुत छटा वहां क्षण-प्रतिक्षण दिखाई पड़ती है। कुछेक लोग व्यर्थ बकवास में लगे हैं कि मैं अपने को अपने गुरु से बड़ा समझता हूं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि पंडितजी को अपना बाप मानते हुए भी उनका विकल्प ढूंढ़ूं। पिता का कोई विकल्प नहीं होता। मेरा दुर्भाग्य है कि वे आज मेरे निकट नहीं हैं, अन्यथा पूछता कि ‘नीला चांद’ की ब्रह्मपुरी आपको कैसी लगती है। उन्हें सुखद आश्चर्य होता कि जो वे जानते हुए भी कह नहीं पाये उसे उनके अब्राह्मण शिष्य ने कहने का प्रयास तो किया। ‘गुरु तल्पं भगम्’ पंडित जी सपने में भी लिख नहीं सकते थे। मैं साक्षी हूं कि उन्होंने ‘पुनर्नवा’ में जब कालिदास को रघुवंशी क्षत्रिय बताया तो बहुत से ब्राह्मण चिढ़े। उन्होंने मुझसे कहा था-तुम भी क्या ऐसा ही समझते हो ? मैंने भीरुता से कहा कि मैं अवतारों, ऋषियों और कवियों के लिए जाति-पांति के बंटखरों का प्रयोग नहीं करता।
मैं परशुराम को ब्राह्मण मानूं और राम को क्षत्रिय तो मैं विश्वचैतन्य के भीतर अमर्ष और मर्यादा के सतत् संघर्ष को समझ नहीं पाऊंगा। मेरे लिए दोनों पूज्य हैं पर साथ ही ये दोनों ही परामानसिक अवतार श्रीकृष्ण से घटकर हैं। असल में हमारा कथा साहित्य इन दिनों ऐसे निकृष्ट बौने समीक्षकों से आक्रान्त है जिनमें 99 प्रतिशत मद है सिर्फ एक प्रतिशत कद। वैसे कोई शून्य प्रतिशत कद कहे तो भी झूठ नहीं होगा। मैं निरन्तर आज के परिवेश से ही टकरा रहा हूं। ‘मंजुशिमा’ और ‘नीला चांद’ पढ़ने वाले अगर दोनों उपन्यासों की समानता को लक्ष्य करते हुए भी मुझे आधुनिक परिवेश से टकराते नहीं देख पाये तो मैं उसे अपनी अभिव्यक्ति की अक्षमता ही मानूंगा, पर इस अक्षमता में 50 प्रतिशत पाठकीय-आलोचकीय अक्षमता भी विद्यमान है जो तृतीय श्रेणी के इतिवृत्तात्मक कथा-साहित्य को मात्र वर्ग-संघर्ष या शिविरवादी संघर्ष का झूठा आईना बताकर उसमें अपने चेहरे की विकृति को देखते हुए भी उसे सृजन का नाम देती है। अब तो काशी त्रयी का वैदिक काल पर आधृत ‘वैश्वानर’ देखेंगे तभी लगेगा कि वहां भी टकराहट आधुनिक परिवेश से ही है या नहीं।
‘वैश्वानार’ अब तक आ गया होता, पर भारत के आधुनिक परिवेश में पिछले एक दशक से जैसा उद्वेलन जन्मा है और जो निरन्तर बदतर रूप लेता जा रहा है, उसने मुझे बहुत तोड़ा। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता से नींद हराम कर रखी है। पूरे विश्व-स्तर पर सभी धर्मों में पुनरुत्थानवादी कट्टरता का कालिया नाग पृथ्वी को निगल पाए या नहीं। पर उसने भारत की मानसी-यमुना को प्रदूषित तो कर ही दिया है। गंगा को अभी भी प्रदूषित कह सकने की मुझमें हिम्मत नहीं है क्योंकि यह यमुना की तरह इन्द्रप्रस्थ जैसी राजधानियों से नहीं जुड़ती। इन्द्रप्रस्थ कहें, पांडवों के पुराने किले में जाएं, लालकोट के भीतर राय पिथौरा के किले को देखें, वहां के भग्नावशेषों के खंडहरों में जाएं, हिन्दू स्थापत्य और मूर्ति रचना के शिल्प को रेशमी कलाबत्तू से बने मुसलमानी पैरहन पर झूलते देखें तो अच्छा लगता है। यही कलाकारिता उन तमाम संगीत शैलियों में भी अपनी सुरभि बिखेरती रही है जो प्राचीन हिन्दू और मुसलमानी पद्धतियों से मिलकर बनी है। पर अब भई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिन्दू के दिल के आयाम को छोटा बनाती जी रही हैं। मुझे मेरठ के दंगे में मरे इंसान की आंखों की जड़ता में ऐसी इबारतें दिखती हैं। उस लाश से एक सवाल उछलता है-‘‘यह कौन था ? क्या आक्रान्ता मुसलमान या गर्वोन्मत्त हिन्दू ? मृत्यु या मृतक की जात नहीं होती। धर्म नहीं होता, पर अब होने लगा है और इतनी ज्यादा तादाद में गुमनाम लाशें बरामद हो रही हैं कि उन पर चुप रहना गुनाह लगता है। हर निर्णायक क्षण में बुद्धिजीवी की चुप्पी या फिर अनावश्यक भंडास की अभिव्यक्ति बौद्धिक दिवालियेपन की शिनाख्त बन जाती है। सच तो यही है कि लिखित शब्द अर्थहीन हो गए हैं, निराधार नारे और अफवाहें सार्थक बनती जा रही हैं। आप पिछले चार दशक से जिस धर्मनिरपेक्षता के खूंटे में देश की नैया को बांधे हुए हैं उसका न रूपाकार है न आयतन। न ही उसकी कोई पहचान है न तो विश्वास और आस्था, जो तूफान में तो कर्णधारों के मन में होनी ही चाहिए।
अगर आपने मन-ही-मन यह निश्चय कर लिया हो कि इतिहास में लौटना प्रतिगामिता है और ऐसा करने वाले वर्तमान से टकराने में कतराते हैं तब तो बहस का सवाल ही नहीं है। आज यदि पूरे विश्व में साहित्य को देखें तो अतीत की ओर दौड़ आपको हतप्रभ कर देगी। आधुनिकता और तकनीकी प्रोन्नति से जन्मे वातावरण में सांस लेना जैसे कठिन हो गया है वैसे ही आज के तथाकथित आधुनिक मूल्यों के कशमकश से घबराकर लोग ऐसे चरित्रों को ढूंढ़ रहे हैं जो अतीत के होते हुए भी हमारे वर्तमान के आदर्श हैं। क्या कारण है पूरे विश्व में आध्यात्मिक साहित्य की ओर रुझानें बढ़ी हैं। वैसे साहित्यिक स्तर पर हम किन्हीं बड़ी कृतियों का नाम न लें तो भी ‘गान विद द विंड’ का पुनर्जन्म हब्शी और श्वेत की समस्याओं के लिए एक सही दस्तावेज क्यों बना ? उसकी प्रासंगिकता इतनी प्रभावी कैसे बनी ? अशोक, चाणक्य, महाभारत के अनेकानेक चरित्र इतने सशक्त मिथक कैसे बन गये। महाभारत तो संस्कृत साहित्यकारों का उपजीव्य ग्रन्थ था ही। 1990 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों में आठ ऐतिहासिक उपन्यासों पर दिये गये। कहने का अर्थ यह है कि आज की कशमकश भरी जिन्दगी से ‘नान्यः पंथा’ (नो एक्जिट) के बीच दम घुटने से बचने के लिए हम पुनः ‘शान्तिः शान्तिः शान्ति’ की ओर चल पड़े हैं।
सर्वत्र प्रदूषण से लड़ने की जागरूकता है। यदि विश्व साहित्य की ओर मुड़ें तो देखेंगे कि यीशु, बुद्ध, गांधी की ओर मुखातिब होकर जनता ने पुनः सलामी दागी है। अफ्रीकी कवियों, खासतौर से नाइजीरिया आदि के बुद्धिजीवियों में ऐतिहासिक प्रतीकों से जुड़ने की प्रक्रिया तीव्र हुई है। करुणा की पुकार बढ़ी है। वैसी ही पुकार श्रीकान्त वर्मा की कविता ‘मगध’ नरेश मेहता की ‘असीरगढ़’ में झलकती है। इन सबका प्रेरणा बिन्दु अपनी-अपनी पहचान को ढूंढ़ने का वह भाव है जो अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकल्प लेकर चला है। यह कार्य अगर भारत में बहुत स्पष्ट रूप से उभरा है तो उसका कारण हमारे इतिहास की समृद्ध परम्परा है। प्राचीनता है। एक गोष्ठी में मुझे रुस्तम सैटिन, नजीर बनारसी और चन्द्रबली सिंह मिल गये। पूछा-‘‘ ‘नीला चांद’ के बाद अब क्या लिख रहे हो।’’ ‘‘हनोज दिल्ली दूर अस्त।’’ मैंने कहा था। ‘‘क्या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर उपन्यास लिख रहे हो ?’’ नजीर साहेब ने पूछा। मैंने कहा, ‘‘बड़ी खुशी होती यदि उन पर लिख पाता, पर अभी तो रुस्तम, नजीर और चंद्रबली सिंह पर लिख रहा हूं।’’ ‘‘मतलब ?’’ तीनों बोले। ‘‘मतलब यह कि क्या आप में से कोई दिल्ली पहुंचा ? क्या दिल्ली आपकी तरफ झांकती है कभी ? क्या दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला अवाम अजनबी शहर में दम नहीं तोड़ रहा है।’’ ‘‘ओफ् ।’’ तीनों ने लम्बी सांस ली।
‘ओफ ।’ आप सब कहिए। अकेले आश्चर्य प्रकट करना मूर्खता है। इसलिए मुंह बांधकर कहिए-‘ओफ् ।’’
इस उपन्यास के अधिकांश चरित्र ऐतिहासिक हैं, पर यदि सचमुच ऐतिहासिक हैं तो मात्र हदबन्दी के रूप में इस उपन्यास में उनका स्थान है। पर असली चरित्र तो वे नहीं हैं। इतिहास पुरुष कोई नहीं है। न कभी था न कभी होगा भवितव्यता है। इसको कहना उतना ही सार्थक लगता है जितना श्रीकृष्ण की गीता की नि संगता या असंगता को गलत कहना। विज्ञान की असंगता में गीता की असंगता की एक झलक है। गणित की असंगता की तरह। या फिर इतिहास की हर काल खण्ड में प्रवेश करती युद्ध और व्यापार की नई धारणाओं को अस्वीकार करना। जिसके पास मानवीय बल है, अच्छे अस्त्र-शस्त्र हैं, अच्छी रणनीति है वह तो सफल होगा ही। जहां-जहां ऐसे साधन रहे हैं, वहां-वहां आक्रमणकारी पीछे हटने को विवश हुए हैं।
यह काल खण्ड अगर प्रो. हबीबुल्ला की पुस्तक से शीर्षक उठाकर कहना चाहूं तो ‘भारत में मुसलमानी सल्तनत की बुनियाद’ के जमाने का है जब सुल्तान अल्तमश और उनके सर्वाधिक सुयोग्य पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी, किन्तु इस काल खण्ड को जानने के लिए अगर पृष्ठभूमि में उतरना अनिवार्य लगे, जो सर्वथा लगना चाहिए तो जुझौती की।
पहाड़ी अधित्यका (पठरा) और उपत्यका (घाटी) में ग्वालियर के सूबेदार मलिक नुसरत तयासी के आक्रमण के साथ-साथ आप भी प्रवेश करें। मैं लाख सफाई दूं। आप यह कहे बिना तो मानेंगे नहीं कि ‘नीला चांद’ की जुझौती फिर प्रकट हो गई। ऐसा सोचना निराधार है। वहां जुझौती या तो मत्तवारिणी में छिपी है या तो अन्त के नेपथ्य में। ‘नीला चांद’ की सही भूमि तो वहां केवल काशी ही रही, जहां आकर कीर्ति वर्मा मध्यकालीन काशी की छवि को देख सका। यह खण्ड ‘कुहरे में युद्ध’ तो पूर्णतः जुझौती पर ही केन्द्रित है। क्यों केन्द्रित हुआ ? कारण कि मुसलमानी आक्रमण से सर्वाधिक रूप से टकराने का कार्य केवल तीन क्षेत्रों में ही हो पाया। सातवीं शताब्दी तक तो इस्लाम सम्पूर्ण मध्य एशिया तथा योरूप में स्पेन तक फैल चुका था। अफ्रीका में नील नदी को लांघ कर दक्षिण तक घुस गया था। कोई भी देश नहीं बचा रास्ते में जो टिक सके। उसी विराट सैलाब को 300 वर्षों तक रोके रखा-काबुल और जाबुल के हिन्दू राजशाहियों ने। महमूद ने इन्हें ई. 1000 के बाद तोड़कर बिखेर दिया और उत्तरापथ की वक्षु-तटीय अर्गला टूटकर छिन्न-भिन्न हो गयी। फिर तो लड़ाई सुरक्षा बन गई। उद्भांड राजधानी बना। शाहाबुशाही चनाब से वाह्लीक तक के हिस्से पर कायम रहे पर अन्ततः इस्लाम के महार्णव में विलीन हो गये। भोला भीम ने सोमनाथ की रक्षा के लिए कई-कई बार आक्रमण का उत्तर प्रत्याक्रमण से दिया पर वह भी पराजित हुआ। किन्तु इन सारी पराजयों में एक अपवाद रही जुझौती जैसा कि प्रो. हबीबुल्ला कहते हैं, ‘‘बुन्देलखण्ड में नुसरत तयासी कोई खास सफल नहीं हो पाया। अपने को सुरक्षित लौट आने को ही वह खुदा का करम मानता रहा।’’ यह लड़ाई कुहरे में क्यों हुई। आप खुद पढ़िये-
चंदेल वंश में एक ही ब्राह्मण वंश के अमात्य कई पीढ़ियों तक उसी पद पर सेवारत रहे। प्रभास देव के वंशज ही मदन वर्मा तक चलते रहे। पर एक-दूसरी भी वंश परम्परा थी जो अपनी आस्था, ईमानदारी और नई से नई समझ-बूझ के कारण चंदेलों से आश्रय पाती रही। वह परम्परा थी कायस्थ वंशोद्भूत जाजुक ठक्कुर की। जिन्हें विद्याधर के पिता गंडदेव ने सर्वाधिकारी नियुक्त किया। इसी वंश में महेश्वर श्रीवास्तव्य का जन्म हुआ जो अप्रतिम सुन्दर और शास्त्रज्ञ थे जिन्हें चंदेल राजवंश के प्रसिद्ध नरेश कीर्ति वर्मा ने कालिंजर का वशिस् बनाया (नीला चाँद में वर्णित) तथा पिपलाहिका ग्राम का स्वामित्व प्रदान किया। इसी राजवंश के सुप्रसिद्ध नरेश परमर्दि देव ने गदाधर को अमात्य नियुक्ति किया। जिनके भाई जौणाधर और मालाधर ने वाण वर्षा से शत्रुओं को छिन्न-भिन्न किया और कालंजर की महिमा अक्षुण्य रखी। उनके पुत्र आल्हु ने नगर प्रतोली की व्यवस्था का भार संभाला। उनके पुत्र हुए शोभन। शोभन के पुत्र अत्यन्त मनोहारी विद्याधर गन्धर्व जैसे सुन्दर वीदन श्रीवास्तव्य हुए जो अनेकानेक गुणों से विभूषित थे। उनके पुत्र हुए वाशेक आनन्द वास्तव्य। वाशेक ने महामात्य का पद संभाला और नरेन्द्र त्रैलोक्य मल्लदेव ने उनके नाम के आदर सहित चरितार्थता प्रदान की। भोजुक जैसे दुर्दान्त शत्रु को वाशेक ने पराजित किया। उसी वाशेक के छोटे भाई पुण्ययशा, उदार, पृथ्वी में सुप्रसिद्ध, सर्वदा लोगों को आनन्द से आनन्दित करने वाले आनन्द वास्तव्य हुए। नृपति त्रैलोक्य मल्ल ने इस अद्भुत भयविहीन व्यक्ति को जयदुर्ग का शासक नियुक्ति किया। आनन्द ने अपराजेय भील, शबर, और पुलिन्दों को वशीभूत कर लिया। उन्हीं के पुत्र थे रुचिर। आनन्द विषयक श्लोक इस प्रकार है-
यही स्थिति आज न केवल साहित्य बल्कि भारतीय समाज के हर क्षेत्र में परिलक्षित होती है। सच तो यह है कि हम अपनी दुर्बलता को स्वीकार करके नये ढंग से अपने को किंचित् बदल कर या वातावरण के अनुकूल अपने को परिवर्तित करके समस्वरता स्थापित करने की प्रक्रिया ही भूल गये हैं। इसी कारण हमारा अतीत शुष्क, वर्तमान दरारों से भरा और भविष्य सूखे पेड़ की तरह निष्पत्र और नंगा लग रहा है। समीक्षा अगर एक बड़ी चीज को समझने में दस वर्ष का समय मांगती है तो मुझे पूर्णतः स्वीकार है, पर मैं उन मुदर्रिसों से लड़ना नहीं चाहता जो विश्वव्यापी कथा-साहित्य से शतप्रतिशत दूर होने को अपना भूषण मानते हैं। अगर आपको निरन्तर सिकुड़ती पृथ्वी की साम्प्रतिक स्थित की सहज प्रतीति नहीं है तो मैं अपने को अपराधी क्यों मानूं ? मेरे लिए प्रेमचन्द अब मंजिल नहीं हैं, उसी तरह मैं प्रसाद को अस्वीकार करना सत्य से आंखे चुराना कहता हूं। आचार्य द्विवेदी के चारों उपन्यास मेरे संबल हैं। क्योंकि प्रसाद और प्रेमचन्द की संधि की एक अद्भुत छटा वहां क्षण-प्रतिक्षण दिखाई पड़ती है। कुछेक लोग व्यर्थ बकवास में लगे हैं कि मैं अपने को अपने गुरु से बड़ा समझता हूं। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि पंडितजी को अपना बाप मानते हुए भी उनका विकल्प ढूंढ़ूं। पिता का कोई विकल्प नहीं होता। मेरा दुर्भाग्य है कि वे आज मेरे निकट नहीं हैं, अन्यथा पूछता कि ‘नीला चांद’ की ब्रह्मपुरी आपको कैसी लगती है। उन्हें सुखद आश्चर्य होता कि जो वे जानते हुए भी कह नहीं पाये उसे उनके अब्राह्मण शिष्य ने कहने का प्रयास तो किया। ‘गुरु तल्पं भगम्’ पंडित जी सपने में भी लिख नहीं सकते थे। मैं साक्षी हूं कि उन्होंने ‘पुनर्नवा’ में जब कालिदास को रघुवंशी क्षत्रिय बताया तो बहुत से ब्राह्मण चिढ़े। उन्होंने मुझसे कहा था-तुम भी क्या ऐसा ही समझते हो ? मैंने भीरुता से कहा कि मैं अवतारों, ऋषियों और कवियों के लिए जाति-पांति के बंटखरों का प्रयोग नहीं करता।
मैं परशुराम को ब्राह्मण मानूं और राम को क्षत्रिय तो मैं विश्वचैतन्य के भीतर अमर्ष और मर्यादा के सतत् संघर्ष को समझ नहीं पाऊंगा। मेरे लिए दोनों पूज्य हैं पर साथ ही ये दोनों ही परामानसिक अवतार श्रीकृष्ण से घटकर हैं। असल में हमारा कथा साहित्य इन दिनों ऐसे निकृष्ट बौने समीक्षकों से आक्रान्त है जिनमें 99 प्रतिशत मद है सिर्फ एक प्रतिशत कद। वैसे कोई शून्य प्रतिशत कद कहे तो भी झूठ नहीं होगा। मैं निरन्तर आज के परिवेश से ही टकरा रहा हूं। ‘मंजुशिमा’ और ‘नीला चांद’ पढ़ने वाले अगर दोनों उपन्यासों की समानता को लक्ष्य करते हुए भी मुझे आधुनिक परिवेश से टकराते नहीं देख पाये तो मैं उसे अपनी अभिव्यक्ति की अक्षमता ही मानूंगा, पर इस अक्षमता में 50 प्रतिशत पाठकीय-आलोचकीय अक्षमता भी विद्यमान है जो तृतीय श्रेणी के इतिवृत्तात्मक कथा-साहित्य को मात्र वर्ग-संघर्ष या शिविरवादी संघर्ष का झूठा आईना बताकर उसमें अपने चेहरे की विकृति को देखते हुए भी उसे सृजन का नाम देती है। अब तो काशी त्रयी का वैदिक काल पर आधृत ‘वैश्वानर’ देखेंगे तभी लगेगा कि वहां भी टकराहट आधुनिक परिवेश से ही है या नहीं।
‘वैश्वानार’ अब तक आ गया होता, पर भारत के आधुनिक परिवेश में पिछले एक दशक से जैसा उद्वेलन जन्मा है और जो निरन्तर बदतर रूप लेता जा रहा है, उसने मुझे बहुत तोड़ा। हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिकता से नींद हराम कर रखी है। पूरे विश्व-स्तर पर सभी धर्मों में पुनरुत्थानवादी कट्टरता का कालिया नाग पृथ्वी को निगल पाए या नहीं। पर उसने भारत की मानसी-यमुना को प्रदूषित तो कर ही दिया है। गंगा को अभी भी प्रदूषित कह सकने की मुझमें हिम्मत नहीं है क्योंकि यह यमुना की तरह इन्द्रप्रस्थ जैसी राजधानियों से नहीं जुड़ती। इन्द्रप्रस्थ कहें, पांडवों के पुराने किले में जाएं, लालकोट के भीतर राय पिथौरा के किले को देखें, वहां के भग्नावशेषों के खंडहरों में जाएं, हिन्दू स्थापत्य और मूर्ति रचना के शिल्प को रेशमी कलाबत्तू से बने मुसलमानी पैरहन पर झूलते देखें तो अच्छा लगता है। यही कलाकारिता उन तमाम संगीत शैलियों में भी अपनी सुरभि बिखेरती रही है जो प्राचीन हिन्दू और मुसलमानी पद्धतियों से मिलकर बनी है। पर अब भई बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हिन्दू के दिल के आयाम को छोटा बनाती जी रही हैं। मुझे मेरठ के दंगे में मरे इंसान की आंखों की जड़ता में ऐसी इबारतें दिखती हैं। उस लाश से एक सवाल उछलता है-‘‘यह कौन था ? क्या आक्रान्ता मुसलमान या गर्वोन्मत्त हिन्दू ? मृत्यु या मृतक की जात नहीं होती। धर्म नहीं होता, पर अब होने लगा है और इतनी ज्यादा तादाद में गुमनाम लाशें बरामद हो रही हैं कि उन पर चुप रहना गुनाह लगता है। हर निर्णायक क्षण में बुद्धिजीवी की चुप्पी या फिर अनावश्यक भंडास की अभिव्यक्ति बौद्धिक दिवालियेपन की शिनाख्त बन जाती है। सच तो यही है कि लिखित शब्द अर्थहीन हो गए हैं, निराधार नारे और अफवाहें सार्थक बनती जा रही हैं। आप पिछले चार दशक से जिस धर्मनिरपेक्षता के खूंटे में देश की नैया को बांधे हुए हैं उसका न रूपाकार है न आयतन। न ही उसकी कोई पहचान है न तो विश्वास और आस्था, जो तूफान में तो कर्णधारों के मन में होनी ही चाहिए।
अगर आपने मन-ही-मन यह निश्चय कर लिया हो कि इतिहास में लौटना प्रतिगामिता है और ऐसा करने वाले वर्तमान से टकराने में कतराते हैं तब तो बहस का सवाल ही नहीं है। आज यदि पूरे विश्व में साहित्य को देखें तो अतीत की ओर दौड़ आपको हतप्रभ कर देगी। आधुनिकता और तकनीकी प्रोन्नति से जन्मे वातावरण में सांस लेना जैसे कठिन हो गया है वैसे ही आज के तथाकथित आधुनिक मूल्यों के कशमकश से घबराकर लोग ऐसे चरित्रों को ढूंढ़ रहे हैं जो अतीत के होते हुए भी हमारे वर्तमान के आदर्श हैं। क्या कारण है पूरे विश्व में आध्यात्मिक साहित्य की ओर रुझानें बढ़ी हैं। वैसे साहित्यिक स्तर पर हम किन्हीं बड़ी कृतियों का नाम न लें तो भी ‘गान विद द विंड’ का पुनर्जन्म हब्शी और श्वेत की समस्याओं के लिए एक सही दस्तावेज क्यों बना ? उसकी प्रासंगिकता इतनी प्रभावी कैसे बनी ? अशोक, चाणक्य, महाभारत के अनेकानेक चरित्र इतने सशक्त मिथक कैसे बन गये। महाभारत तो संस्कृत साहित्यकारों का उपजीव्य ग्रन्थ था ही। 1990 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों में आठ ऐतिहासिक उपन्यासों पर दिये गये। कहने का अर्थ यह है कि आज की कशमकश भरी जिन्दगी से ‘नान्यः पंथा’ (नो एक्जिट) के बीच दम घुटने से बचने के लिए हम पुनः ‘शान्तिः शान्तिः शान्ति’ की ओर चल पड़े हैं।
सर्वत्र प्रदूषण से लड़ने की जागरूकता है। यदि विश्व साहित्य की ओर मुड़ें तो देखेंगे कि यीशु, बुद्ध, गांधी की ओर मुखातिब होकर जनता ने पुनः सलामी दागी है। अफ्रीकी कवियों, खासतौर से नाइजीरिया आदि के बुद्धिजीवियों में ऐतिहासिक प्रतीकों से जुड़ने की प्रक्रिया तीव्र हुई है। करुणा की पुकार बढ़ी है। वैसी ही पुकार श्रीकान्त वर्मा की कविता ‘मगध’ नरेश मेहता की ‘असीरगढ़’ में झलकती है। इन सबका प्रेरणा बिन्दु अपनी-अपनी पहचान को ढूंढ़ने का वह भाव है जो अपनी जड़ों की ओर लौटने का संकल्प लेकर चला है। यह कार्य अगर भारत में बहुत स्पष्ट रूप से उभरा है तो उसका कारण हमारे इतिहास की समृद्ध परम्परा है। प्राचीनता है। एक गोष्ठी में मुझे रुस्तम सैटिन, नजीर बनारसी और चन्द्रबली सिंह मिल गये। पूछा-‘‘ ‘नीला चांद’ के बाद अब क्या लिख रहे हो।’’ ‘‘हनोज दिल्ली दूर अस्त।’’ मैंने कहा था। ‘‘क्या ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया पर उपन्यास लिख रहे हो ?’’ नजीर साहेब ने पूछा। मैंने कहा, ‘‘बड़ी खुशी होती यदि उन पर लिख पाता, पर अभी तो रुस्तम, नजीर और चंद्रबली सिंह पर लिख रहा हूं।’’ ‘‘मतलब ?’’ तीनों बोले। ‘‘मतलब यह कि क्या आप में से कोई दिल्ली पहुंचा ? क्या दिल्ली आपकी तरफ झांकती है कभी ? क्या दिल्ली की सड़कों पर चलने वाला अवाम अजनबी शहर में दम नहीं तोड़ रहा है।’’ ‘‘ओफ् ।’’ तीनों ने लम्बी सांस ली।
‘ओफ ।’ आप सब कहिए। अकेले आश्चर्य प्रकट करना मूर्खता है। इसलिए मुंह बांधकर कहिए-‘ओफ् ।’’
इस उपन्यास के अधिकांश चरित्र ऐतिहासिक हैं, पर यदि सचमुच ऐतिहासिक हैं तो मात्र हदबन्दी के रूप में इस उपन्यास में उनका स्थान है। पर असली चरित्र तो वे नहीं हैं। इतिहास पुरुष कोई नहीं है। न कभी था न कभी होगा भवितव्यता है। इसको कहना उतना ही सार्थक लगता है जितना श्रीकृष्ण की गीता की नि संगता या असंगता को गलत कहना। विज्ञान की असंगता में गीता की असंगता की एक झलक है। गणित की असंगता की तरह। या फिर इतिहास की हर काल खण्ड में प्रवेश करती युद्ध और व्यापार की नई धारणाओं को अस्वीकार करना। जिसके पास मानवीय बल है, अच्छे अस्त्र-शस्त्र हैं, अच्छी रणनीति है वह तो सफल होगा ही। जहां-जहां ऐसे साधन रहे हैं, वहां-वहां आक्रमणकारी पीछे हटने को विवश हुए हैं।
यह काल खण्ड अगर प्रो. हबीबुल्ला की पुस्तक से शीर्षक उठाकर कहना चाहूं तो ‘भारत में मुसलमानी सल्तनत की बुनियाद’ के जमाने का है जब सुल्तान अल्तमश और उनके सर्वाधिक सुयोग्य पुत्र नासिरुद्दीन की मृत्यु हो चुकी थी, किन्तु इस काल खण्ड को जानने के लिए अगर पृष्ठभूमि में उतरना अनिवार्य लगे, जो सर्वथा लगना चाहिए तो जुझौती की।
पहाड़ी अधित्यका (पठरा) और उपत्यका (घाटी) में ग्वालियर के सूबेदार मलिक नुसरत तयासी के आक्रमण के साथ-साथ आप भी प्रवेश करें। मैं लाख सफाई दूं। आप यह कहे बिना तो मानेंगे नहीं कि ‘नीला चांद’ की जुझौती फिर प्रकट हो गई। ऐसा सोचना निराधार है। वहां जुझौती या तो मत्तवारिणी में छिपी है या तो अन्त के नेपथ्य में। ‘नीला चांद’ की सही भूमि तो वहां केवल काशी ही रही, जहां आकर कीर्ति वर्मा मध्यकालीन काशी की छवि को देख सका। यह खण्ड ‘कुहरे में युद्ध’ तो पूर्णतः जुझौती पर ही केन्द्रित है। क्यों केन्द्रित हुआ ? कारण कि मुसलमानी आक्रमण से सर्वाधिक रूप से टकराने का कार्य केवल तीन क्षेत्रों में ही हो पाया। सातवीं शताब्दी तक तो इस्लाम सम्पूर्ण मध्य एशिया तथा योरूप में स्पेन तक फैल चुका था। अफ्रीका में नील नदी को लांघ कर दक्षिण तक घुस गया था। कोई भी देश नहीं बचा रास्ते में जो टिक सके। उसी विराट सैलाब को 300 वर्षों तक रोके रखा-काबुल और जाबुल के हिन्दू राजशाहियों ने। महमूद ने इन्हें ई. 1000 के बाद तोड़कर बिखेर दिया और उत्तरापथ की वक्षु-तटीय अर्गला टूटकर छिन्न-भिन्न हो गयी। फिर तो लड़ाई सुरक्षा बन गई। उद्भांड राजधानी बना। शाहाबुशाही चनाब से वाह्लीक तक के हिस्से पर कायम रहे पर अन्ततः इस्लाम के महार्णव में विलीन हो गये। भोला भीम ने सोमनाथ की रक्षा के लिए कई-कई बार आक्रमण का उत्तर प्रत्याक्रमण से दिया पर वह भी पराजित हुआ। किन्तु इन सारी पराजयों में एक अपवाद रही जुझौती जैसा कि प्रो. हबीबुल्ला कहते हैं, ‘‘बुन्देलखण्ड में नुसरत तयासी कोई खास सफल नहीं हो पाया। अपने को सुरक्षित लौट आने को ही वह खुदा का करम मानता रहा।’’ यह लड़ाई कुहरे में क्यों हुई। आप खुद पढ़िये-
चंदेल वंश में एक ही ब्राह्मण वंश के अमात्य कई पीढ़ियों तक उसी पद पर सेवारत रहे। प्रभास देव के वंशज ही मदन वर्मा तक चलते रहे। पर एक-दूसरी भी वंश परम्परा थी जो अपनी आस्था, ईमानदारी और नई से नई समझ-बूझ के कारण चंदेलों से आश्रय पाती रही। वह परम्परा थी कायस्थ वंशोद्भूत जाजुक ठक्कुर की। जिन्हें विद्याधर के पिता गंडदेव ने सर्वाधिकारी नियुक्त किया। इसी वंश में महेश्वर श्रीवास्तव्य का जन्म हुआ जो अप्रतिम सुन्दर और शास्त्रज्ञ थे जिन्हें चंदेल राजवंश के प्रसिद्ध नरेश कीर्ति वर्मा ने कालिंजर का वशिस् बनाया (नीला चाँद में वर्णित) तथा पिपलाहिका ग्राम का स्वामित्व प्रदान किया। इसी राजवंश के सुप्रसिद्ध नरेश परमर्दि देव ने गदाधर को अमात्य नियुक्ति किया। जिनके भाई जौणाधर और मालाधर ने वाण वर्षा से शत्रुओं को छिन्न-भिन्न किया और कालंजर की महिमा अक्षुण्य रखी। उनके पुत्र आल्हु ने नगर प्रतोली की व्यवस्था का भार संभाला। उनके पुत्र हुए शोभन। शोभन के पुत्र अत्यन्त मनोहारी विद्याधर गन्धर्व जैसे सुन्दर वीदन श्रीवास्तव्य हुए जो अनेकानेक गुणों से विभूषित थे। उनके पुत्र हुए वाशेक आनन्द वास्तव्य। वाशेक ने महामात्य का पद संभाला और नरेन्द्र त्रैलोक्य मल्लदेव ने उनके नाम के आदर सहित चरितार्थता प्रदान की। भोजुक जैसे दुर्दान्त शत्रु को वाशेक ने पराजित किया। उसी वाशेक के छोटे भाई पुण्ययशा, उदार, पृथ्वी में सुप्रसिद्ध, सर्वदा लोगों को आनन्द से आनन्दित करने वाले आनन्द वास्तव्य हुए। नृपति त्रैलोक्य मल्ल ने इस अद्भुत भयविहीन व्यक्ति को जयदुर्ग का शासक नियुक्ति किया। आनन्द ने अपराजेय भील, शबर, और पुलिन्दों को वशीभूत कर लिया। उन्हीं के पुत्र थे रुचिर। आनन्द विषयक श्लोक इस प्रकार है-
तस्यानुजः पुण्ययशा उदारः आनन्दनामा प्रथितः पृथिव्याम्
सदैव लोकं मदयन्तमाराह्यं सतपत्थयनामानुदाहरन्ति
भियामभूमिः विगणज्ज चैनं दुर्दाधिकारं नृपतिः प्रचके
आज्ञा करान्यल्लिनिवासनीयं चकार भिल्लास्वसवरान्पुलिन्दान
सदैव लोकं मदयन्तमाराह्यं सतपत्थयनामानुदाहरन्ति
भियामभूमिः विगणज्ज चैनं दुर्दाधिकारं नृपतिः प्रचके
आज्ञा करान्यल्लिनिवासनीयं चकार भिल्लास्वसवरान्पुलिन्दान
यह शिलालेख आनन्द वाशेक के पौत्र सुभट ने लिखवाया जो भोजवर्मदेव का
कोशाधिपति था और उसे अजयगढ़ के पास संस्थापित कराया। प्रश्न होता है कि
अगर वह जयदुर्ग अजयगढ़ ही था तो क्या त्रैलोक्य मल्ल देव को वह नाम मालूम
नहीं था। भोजवर्म देव को क्या अजयगढ़ भूल गया। बहरहाल मेरी कल्पना का
जयदुर्ग कहीं और है। मैं इतिहास में एक झूठ और शामिल कर रहा हूं जिसके लिए
कोई क्षमा-याचना अनावश्यक है। जब सही जगह ज्ञात होगी तो लोग मेरी कल्पना
को क्षमा कर देंगे क्योंकि मैं भूगोल, इतिहास और पुरातत्व से मात्र
प्रामाणिकता ही नहीं लेता, उस अज्ञात नाड़ी की धड़कन भी सुनता हूं जो कभी
झूठ नहीं बोलती।
अब यह प्रश्न है। बिना अर्थ के सोचने की बात है। चन्देलवंश के ब्राह्मण अमात्यों ने अपने वंश के लोगों के लिए कोई शिलालेख नहीं लगाया। चन्देल शिलालेखों में धंग देव के प्रधानामात्य प्रभास देव का नाम ही नहीं गोत्र, विद्या, कुलशील सब लिखा है। वैसे ही अन्य लोगों के भी उल्लेख हैं। बिना लंबी-चौड़ी प्रशस्ति के। अचानक कायस्थ अमात्यों के उदय के साथ उन्हीं के परवर्ती उत्तराधिकारी ने जो आनन्द का पौत्र और भोजवर्मदेव का भांडागारिक था ऐसा लेख क्यों लिखवाया। उस प्रदेश के जिसे आज छत्तीसगढ़ कहते हैं गांवों को या कहें तो गढ़ियों को इतना महत्त्व क्यों दिया गया। ‘‘वहां निरन्तर वेद ध्वनि से शिक्षा प्रारम्भ होती, यज्ञ हवन होते फिर नाना शास्त्रों का अध्ययन होता।’’ शिलालेख तो कहता है-‘‘इस जनपद की पवित्रता तो इसी में निहित है कि यहां वास्तुदेव ने इन छत्तीसगढ़ियों को अपना गृह क्षेत्र बनाया ताकि द्विजकुलोद्भूत लोग यहां प्रलय तक आबाद रहें।’’ एक श्लोक तो ऐसा है जैसे ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा स्वरूप लिखा गया है-मैं केवल इस तथ्य के पीछे विद्यमान उस प्रवृत्ति को देख रहा हूं जहां से हमारे सामाजिक आचार-विचार को ठेस लगी होगी। ब्राह्मण ही ज्ञान-विज्ञान के स्तंभ और वितान हैं, इसे अस्वीकार करते हुए लेखक वर्ग के लोग प्रतिस्पर्धापूर्वक ब्राह्मणत्व को अस्वीकार करते हैं क्योंकि जिस ज्ञान को परम्परा से वे पाते रहे उसी को शूद्र कहे जाने वाले कायस्थों ने प्राप्त किया है। इसके पीछे मृच्छकटिक का वह श्लोक भी ध्यान देने योग्य है जिसमें कायस्थों को शूद्र से भी अधिक नीच, वेश्या और गधे से हीन बताया गया है। इसी दृष्टि में से हमें मध्यकालीन जीर्ण-शीर्ण वर्ण-व्यवस्था को मसल देने वाले उन बौद्धिकों का स्वागत करना चाहिए जिन्होंने वर्ण शुद्धता की भावुकता को तोड़कर नये से नये ज्ञान और तकनीकों को अंगीकार किया। वाशेक उस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उठने वाला सबसे सशक्त और आक्रामक राजपुरुष है जो दकियानूस हिन्दू रूढ़िवादिता को तोड़ता है और विदेश से आई नई जाति की नई रणनीति को सीखता है ताकि शत्रु को उसी की शैली में उत्तर दे सके। अगर वाशेक आनन्द जुझौती में न होता तो छद्म युद्ध का प्रयोग, वे लोग कैसे कर पाते जो बाहर से आने वालों को जानते तक नहीं थे। कायस्थ बौद्धिकों ने इसी ललक का परिचय अंग्रेजी शासन के दिनों में भी दिया और आज भी वे अगर बौद्धिक वर्ग में अपनी अग्रता कायम किये हैं तो वह इसी परम्परा की देन है जिसे वाशेक आनन्द ने व्यावहारिक रूप दिया था।
अब यह प्रश्न है। बिना अर्थ के सोचने की बात है। चन्देलवंश के ब्राह्मण अमात्यों ने अपने वंश के लोगों के लिए कोई शिलालेख नहीं लगाया। चन्देल शिलालेखों में धंग देव के प्रधानामात्य प्रभास देव का नाम ही नहीं गोत्र, विद्या, कुलशील सब लिखा है। वैसे ही अन्य लोगों के भी उल्लेख हैं। बिना लंबी-चौड़ी प्रशस्ति के। अचानक कायस्थ अमात्यों के उदय के साथ उन्हीं के परवर्ती उत्तराधिकारी ने जो आनन्द का पौत्र और भोजवर्मदेव का भांडागारिक था ऐसा लेख क्यों लिखवाया। उस प्रदेश के जिसे आज छत्तीसगढ़ कहते हैं गांवों को या कहें तो गढ़ियों को इतना महत्त्व क्यों दिया गया। ‘‘वहां निरन्तर वेद ध्वनि से शिक्षा प्रारम्भ होती, यज्ञ हवन होते फिर नाना शास्त्रों का अध्ययन होता।’’ शिलालेख तो कहता है-‘‘इस जनपद की पवित्रता तो इसी में निहित है कि यहां वास्तुदेव ने इन छत्तीसगढ़ियों को अपना गृह क्षेत्र बनाया ताकि द्विजकुलोद्भूत लोग यहां प्रलय तक आबाद रहें।’’ एक श्लोक तो ऐसा है जैसे ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा स्वरूप लिखा गया है-मैं केवल इस तथ्य के पीछे विद्यमान उस प्रवृत्ति को देख रहा हूं जहां से हमारे सामाजिक आचार-विचार को ठेस लगी होगी। ब्राह्मण ही ज्ञान-विज्ञान के स्तंभ और वितान हैं, इसे अस्वीकार करते हुए लेखक वर्ग के लोग प्रतिस्पर्धापूर्वक ब्राह्मणत्व को अस्वीकार करते हैं क्योंकि जिस ज्ञान को परम्परा से वे पाते रहे उसी को शूद्र कहे जाने वाले कायस्थों ने प्राप्त किया है। इसके पीछे मृच्छकटिक का वह श्लोक भी ध्यान देने योग्य है जिसमें कायस्थों को शूद्र से भी अधिक नीच, वेश्या और गधे से हीन बताया गया है। इसी दृष्टि में से हमें मध्यकालीन जीर्ण-शीर्ण वर्ण-व्यवस्था को मसल देने वाले उन बौद्धिकों का स्वागत करना चाहिए जिन्होंने वर्ण शुद्धता की भावुकता को तोड़कर नये से नये ज्ञान और तकनीकों को अंगीकार किया। वाशेक उस वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उठने वाला सबसे सशक्त और आक्रामक राजपुरुष है जो दकियानूस हिन्दू रूढ़िवादिता को तोड़ता है और विदेश से आई नई जाति की नई रणनीति को सीखता है ताकि शत्रु को उसी की शैली में उत्तर दे सके। अगर वाशेक आनन्द जुझौती में न होता तो छद्म युद्ध का प्रयोग, वे लोग कैसे कर पाते जो बाहर से आने वालों को जानते तक नहीं थे। कायस्थ बौद्धिकों ने इसी ललक का परिचय अंग्रेजी शासन के दिनों में भी दिया और आज भी वे अगर बौद्धिक वर्ग में अपनी अग्रता कायम किये हैं तो वह इसी परम्परा की देन है जिसे वाशेक आनन्द ने व्यावहारिक रूप दिया था।
13, गुरुधाम कालोनी
वाराणसी-221010
-शिवप्रसाद सिंह
धन्वतरि जयन्ती
वाराणसी-221010
-शिवप्रसाद सिंह
धन्वतरि जयन्ती
23.10.92
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i